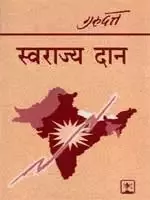|
राजनैतिक >> स्वराज्य दान स्वराज्य दानगुरुदत्त
|
430 पाठक हैं |
||||||
राजनीति पर आधारित उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
स्वराज्य-दान
‘‘भूल जाना मनुष्यता की बात नहीं। मनुष्यों में और अन्य
प्राणियों में स्मरण-शक्ति का ही अन्तर है। मनुष्य तो उन्नति कर रहा है
किन्तु अन्य प्राणी उन्नति नहीं कर रहे हैं। इसका कारण स्मरण-शक्ति ही है।
पूर्व अनुभवों का मनन करके ही विचारों को आगे ले जाया जा सकता है। अन्य
प्राणी अनेक अनुभवों को भूल जाते हैं, इससे वे अपनी भूलों को सुधार नहीं
सकते। मनुष्य अपनी देखी-सुनी, अनुभव अथवा विचार की हुई बातों का स्मरण
करके ही उन्नति के मार्ग पर चलता आ रहा है। लिखने की विद्या का आविष्कार
भी तो स्मरण-क्रिया को और अधिक स्थायी करने के लिए ही किया गया है।
‘‘यह सब जानते हुए भी आप मुझे क्यों कहते हैं कि जो अन्याय और अत्याचार मुझ पर मेरे भाई-बन्धुओं पर हुए हैं, मैं उनको भूल जाऊँ ? भूल जाऊँगा फिर उनकी पुनरावृत्ति कैसे की जा सकेगी ?’’
यह वार्तालाप नई दिल्ली में कर्जन रोड पर एक कोठी के ड्राइंग-रूम में, एक गद्देदार आराम-कुर्सी पर बैठ हुए अधेड़ आयु के पुरुष और उसके सामने खड़े हुए एक युवक में हो रहा था। युवक की आयु लगभग पच्चीस वर्ष की प्रतीत होती थी। युवक ने यह बात उस अधेड़ आयु के पुरुष के इस कथन के उत्तर में कही थी—
‘‘नरेन्द्र, देखो, तुम्हारी माता का देहान्त हो चुका है। तुम दो वर्ष के थे जब तुम्हारे पिता मारे गए थे। तब से तुम्हारी माता ने बहुत धैर्य और परिश्रम से तुम्हारा पालन-पोषण कर तुम्हें इतना बड़ा किया है। यह बीस-बाईस वर्ष की तपस्या किसलिए की गई थी ? इसलिए ही न कि तुम पढ़-लिखकर बड़े हो जाओ, विवाह करो और अपने पिता का वंश चलाओ। तुम्हारे लिए यही अवसर है कि तुम अपनी माँ की इच्छा पूर्ण कर उसकी पवित्र स्मृति को चिरस्थायी बनाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूढ़ी है। वह पढ़ी-लिखी है, सुन्दर है, सुशील है, सुघड़ है और अति मीठा बोलने वाली है। एक बार चलकर लड़की को देख लो। देखो, माँ के परिश्रम का स्वाभाविक फल यही है। वह बेचारी जीती होती तो बहू लाने की बात सुनकर कितना आनन्द का अनुभव करती।’’
युवक का कहना था कि, ‘‘चाचा जी, आप नहीं जानते कि माता जी ने मुझे पढ़ाया-लिखाया क्यों है। आप समझते हैं कि पिताजी का वंश को चलाना ही उनके इस प्रयास का ध्येय था। यह तो बहुत छोटी बात है। वे इस प्रकार के छोटे विचारों की स्त्री नहीं थीं। मैं आपको बताता हूँ। मैंने मैट्रिक पास करने के पाश्चात् एक बार उनसे कहा था, ‘‘माँ, तुम्हें मेरे लिए गरीबी सहन करनी पड़ रही है; यदि तुम कहो तो मैं कहीं नौकरी कर लूँ। अब कहीं-न-कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी।’
‘‘माता जी ने मेरी बात सुन, माथे पर त्योरी चढ़ाकर कहा था, ‘‘देखो, नरेन्द्र, तुम्हारे चाचा जो कुछ भेजते हैं उससे तो तुम्हारी फीस और किताबों का खर्च भी नहीं चलता। घर और शेष तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए मुझे कपड़े सीने का काम करना पड़ता है। तुम्हें अखाड़े में कसरत करके आने पर बादाम और दूध देने तथा तुम्हारे कपड़े और अन्य आवश्यक बातों के लिए मैं जो दिन-रात मेहनत कर रही हूँ वह क्या केवल तुम्हारे तीस रुपये मासिक का क्लर्क बनाने के लिए है ? तुम्हारे खाने, पहनने, पुस्तकों और स्कूल इत्यादि की फीस के लिए, रात-रात-भर बैठकर लोगों के कपड़े सी-सीकर, मैं अपनी आँखें इसलिए खराब नहीं कर रही कि तुम विदेशी सरकार की नौकरी करने के योग्य हो जाओ। देखो, बेटा, मैं तुम्हें सबल और योग्य इसलिए बना रही हूँ कि तुम अपने पिता और मेरे अपमान का बदला ले सको। मैं आज फिर तुम्हें उस अपमान की कहानी सुनाती हूँ।
‘सन् 1919, अप्रैल मास के दिन थे। महात्मा गांधी पंजाब आ रहे थे और पंजाब सरकार ने उन्हें आने से रोक दिया था। जब उन्होंने आने का हठ किया तो सरकार ने उन्हें बन्दी बना लिया। लोगों ने हड़ताल कर दी, जो कई दिन तक रही। उस समय तुम दो वर्ष के थे। तुम्हारे पिता हाल बाजार में बिसाती की दुकान करते थे। वे भी दुकान बन्द करके घर आ बैठे।
‘वैशाख की संक्रांति थी। उनके मन में आया कि ‘दरबार साहब’ में स्नान तथा दर्शन कर आवें। मैं भी साथ जाती, परन्तु तुम्हारी बहन, राधा, पेट में थी। अतएव मैं और तुम घर पर ही रहे और वे लोटा लेकर दरबार साहब चले गए। उनका विचार था कि अमृतसर के जल का लोटा भरकर मेरे और तुम्हारे लिए लावेंगे।
‘वे गए और फिर नहीं आए। सायंकाल तक मैं प्रतीक्षा करती रही। उनके न आने पर मैं बेचैन हो उठी। मुहल्ले में हल्ला मच गया कि जलियांवाला बाग में लोग जलसा कर रहे थे कि फौज ने गोली चलाकर सहस्रों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मेरा माथा ठनका। यद्यपि वे कभी ऐसे जलसे-जुलूसों में सम्मिलित नहीं होते थे, फिर भी मुझे विश्वास-सा होने लगा था कि वे वहीं पर मारे गए हैं। मैंने तुम्हें पड़ोसन के घर छोड़ा और जलियांवाला बाग को चल पड़ी। मुहल्ले के लोगों ने मना किया, पर मैं उतावली हो रही थी। वे कहते थे कि संध्या होने वाली है और ‘कर्फ्यू-आर्डर’ लगा हुआ है, किसी फौजी ने देख लिया तो वह गोली से मार डालेगा। मैं भगवान् के भरोसे पर थी। बाजार सुनसान पड़े थे। कोई पक्षी तक भी फड़क नहीं रहा था। मैं मकानों के साथ-साथ होती हुई चली गई। मेरे मन में अपने लिए भय नहीं था। मुझे विश्वास-सा हो रहा था कि तुम्हारे पिता जीवित नहीं हैं। जीवित होते तो अवश्य लौट आते। इस बात का निश्चय करना मेरे लिए नितान्त आवश्यक था। मैं चलती गई। तब तक प्रकाश पर्याप्त था, मैं वहाँ जा पहुँची।
‘जलियांवाले अहाते में जाने के दो मार्ग हैं। एक बड़ा फाटक-सा है, और दूसरे को तो केवल खिड़की ही कहना चाहिए। मैं फाटक के मार्ग से भीतर गई थी। सामने हाय-हाय मची हुई थी। हजारों लोगों के मुख से आर्त्तनाद निकल रहा था। कोई-कोई विरला उनमें खड़ा अपनी सम्बन्धियों को पहचान रहा था। ये अपने सम्बन्धियों को ढूँढ़ने वाले, कभी-कभी शवों को घसीटकर इधर-उधर करते थे। सूर्यास्त होने में कुछ मिनट ही रह गए थे और ढूँढ़ने वाले अनुभव कर रहे थे कि शीघ्र ही उनको लौट जाना है। सूर्यास्तके पश्चात् शव ले जाना तो एक तरफ रहा घर पहुँचना भी भय-रहित नहीं रह जावेगा।
‘मैं इस भयानक दृश्य को देख हतोत्साहित हो गई। मेरा दिल बैठने लगा और मैं अपनी टाँगों पर खड़ी न रह सकी। जहाँ मैं बैठी थी वहाँ समीप ही एक घायल पड़ा था। वह मुझे देखते ही पानी माँगने लगा। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी जाँघ में गोली लगी थी और वह हिल नही सकता था। वहाँ न लोटा था, न कुआँ। पानी लाती भी तो कहाँ से ? मेरे आँसू बहने लगे।
‘जिन ढूँढ़नेवालों को अपने आदमी मिल जाते थे वे उन्हें उठाकर चले जा रहे थे। उनमें से एक आदमी मुझे चुपचाप बैठे और रोते देख बोला, ‘माई, जल्दी चली जाओ। साढ़े सात बज रहे हैं। ‘कर्फ्यू आर्डर’ हो गया है’। इतना कहते-कहते वह रुक गया। वह खड़ा हो गया। शायद वह मेरी गर्भावस्था जान गया था और मन में कुछ सोचकर पूछने लगा, ‘‘तुम इसे कहाँ ले जाना चाहती हो ?’ उसने समीप पड़े घायल को मेरा सम्बन्धी समझ लिया था।
‘मैंने कहा, ‘इसे थोड़ा पानी पिला दो।’ मैं उसे होंठों पर जुबान फेरते देख तुम्हारे पिता के विषय में भूल गई थी। वह आदमी विचार में पड़ गया। बोला, ‘बहन, यहाँ पानी नहीं है। चलो, मैं इसे उठाकर ले चलता हूँ। आपको इसे कहाँ ले चलना है ?’
‘मुझे तुम्हारे पिता की याद आ गई। मैंने कहा, ‘‘इसे मैं नहीं जानती, मैं तो किसी और को ढूँढ़ने आयी थी।’
‘वह मिला ?’
‘नहीं, अभी नहीं। मुझ में यह सब ढूँढ़ने की हिम्मत नहीं रही।’
‘वह आपका क्या है ?’
‘मेरे पति हैं।’
‘उस भले पुरुष के मुख पर दया की झलक दिखाई दे रही थी। वह बोली, ‘चलो, उसे भी देख लो, बहन ! शायद उसे भी पानी की आवश्यकता हो।’
‘उसने मुझे आश्रय दे उठाया और हम ढूँढ़ने लगे। अहाते के एक ओर एक दीवार थी और सबसे अधिक लाशें उसी दीवार के समीप थी। एक स्थान पर लाशों का ढेर लगा था। मैं ढूँढ़ती हुई वहाँ पहुँची। उफ ! कितना भयंकर दृश्य। अब भी स्मरण आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक-एक शव को पकड़कर मुख देखती थी और पहचानती थी। जब निश्चय हो जाता था कि तुम्हारे पिता नहीं है, तो उन्हें घसीटकर एक तरफ कर देती थी और फिर दूसरों को देखती थी। सभी लोग इस प्रकार कर रहे थे। इस पर भी यह कार्य इतनी कठोरतापूर्ण था कि साधारण परिस्थिति में कोई अति कठोर-हृदय भी शायद वैसा ही कर सकता। मुझसे यह कुछ न हो सकता, यदि वह भला पुरुष मेरी सहायता न कर रहा होता। आखिर लाशों के एक ढेर के नीचे उनका शव निकला। उनके सिर में गोली लगी थी और खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए थे। उनका मुख पहचाना नहीं जाता था परन्तु कपड़ों से पहचान गई थी। उनको देख अपनी क्षीण सूत्रवत् आशा, कि शायद वे भी घायल पड़े हों, विलुप्त हुई जान में गश खाकर गिर पड़ी।
‘जब मुझे चेतना हुई तो वही भला आदमी मुख पर पान के छींटे लगा रहा था। अँधेरा पर्याप्त हो चुका था इसलिए पहले तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकी। इस समय उसके साथ एक आदमी था। वह हाथ में एक गगरा पानी लिये खड़ा था। जब पहचान गई तो मैंने पूछा, ‘उसे पानी पिलाया है, भैया ?’
‘बहिन जब तुम बेहोश हो गई थीं मैं पानी लेने चला गया था। मैंने विचार किया था कि तुम्हें सचेत करने के लिए भी तो पानी चाहिए। बाजार में कुआँ तो था पर गगरा नहीं था। एक मकान का दरवाजा खटखटाया और लोटा और गगरा माँगा। उस घर वालों ने एकदम इन्कार कर दिया। कई स्थानों पर यत्न करते-करते ये सज्जन मिले। घर पर ये अकेले थे। जब मैंने अपना आशय वर्णन किया, तो दाँतों को पीसते हुए गगरा और लोटा ले मेरे साथ चल पड़ा। इस सब प्रयत्न में एक घण्टा लग गया है, और इस बीच वह आदमी चल बसा है। अब उसकी सहायता नहीं कर सकते।’
‘मैं पगली-सी इन बातों को सुन रही थी। मुझे न तो अपनी जान का भय रह गया था और न ही उनके भय का अनुमान लगाने की मुझमें शक्ति रह गई थी। गगरा लिये हुए आदमी ने दूसरे घायलों को पानी पिलाना आरम्भ कर दिया। एक गगरे से वहाँ क्या हो सकता था। देखते-देखते पानी समाप्त हो गया। अब वह हमारे समीप आया और बोला, ‘माताजी, अब चलना चाहिए। आपको घर पहुँचा दूँ तो इनके लिए और जल का प्रबन्ध करूँ।’
‘मैंने अपनी गली का नाम बताया तो उन दोनों ने तुम्हारे पिता का शव कंधों पर उठा लिया और मुझे साथ ले घर पहुँचा गए। उस रात यद्यपि ‘कर्प्यू आर्डर’ लगा हुआ था, परन्तु तमाम अमृतसर में एक भी पुलिस तथा फौज का सिपाही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि ये लोग डर रहे थे कि उनके लिए शहर के भीतर आना मौत का आवाहन करना है। इस झूठे भय के कारण लोगों को रात के समय अपने घायल सम्बन्धी अथवा उनकी लाशें जलियांवाला बाग से ले जाने का अवसर मिल गया। प्रातःकाल तक कुछ लावारिस शवों के अतिरिक्त सहस्रों घायल तथा मृत वहाँ से ले जाए जा चुके थे।
‘दूसरे दिन केवल पाँच आदमियों की सहायता से तुम्हारे पिता का दाह संस्कार किया गया। श्मशान-भूमि तक जाने के लिए भी पाँच से अधिक लोगों का एकत्रित होना रोक दिया गया था।
‘जलियांवाला बाग में गोलियाँ चलाने वाला कर्नल डायर था। उस निर्दयी ने निहत्थे लोगों पर जो शान्तिपूर्वक जलसा कर रहे थे, तब तक गोलियां चलाई जब तक कि उसके सिपाहियों के कारतूस समाप्त नहीं हो गए।’
‘बात यहीं समाप्त नहीं हुई। हमारी गली के बाहर फौजियों का पहरा बैठ गया। वे आने-जाने वालों को पेट के बल रेंगने को बाध्य करते थे। हमारी गली वालों ने इस अपमान को न सह सकने के कारण घर से निकलना बन्द कर दिया। दुर्भाग्य से हमारे घर में रसद-पानी समाप्त हो गया। गली में प्रायः सब घरों का ऐसा ही हाल था। मैंने एक पड़ोसी से कुछ ला देने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। मैंने कहा, ‘‘नन्हा भूख से बिलख-बिलखकर रो रहा है।’ वह पड़ोसी चुप रहा उसके मुख पर विवशका की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। तुम्हें कुछ खाये चौबीस घंटे से ऊपर हो चुके थे। एक-दो बार तुम्हें पानी में चीनी घोलकर दिया। उससे तुम्हारी तृप्ति नहीं होती थी और फिर चीनी भी समाप्त हो गई थी। नगर में एक सप्ताह से ऊपर दूकानें बन्द रही थीं, और जब दूकानें खुलीं तो गली के बाहर यह आफत आ बैठी। परिणामस्वरूप उस गली में रहने वाले प्रायः सब फाके कर रहे थे। मैं माँगती भी तो किससे ? तब तुम बहुत रोने लगे तो मैंने इस अपमान को सहन करने की ठान ली। मेरे मन में पागलपन समा रहा था। मैं सोचती थी कि मैंने, तुमने और तुम्हारी बहन ने, जो अभी पेट में थी, उन लोगों का क्या बिगाड़ा है। वे मुझे रेंगेने के लिए क्यों कहेंगे ? मैंने कपड़े बदल लिये। सलवार, कुर्ता और दुपट्टा ओढ़ और हाथ में सामान के लिए चादर लेकर चल पड़ी।
‘‘यह सब जानते हुए भी आप मुझे क्यों कहते हैं कि जो अन्याय और अत्याचार मुझ पर मेरे भाई-बन्धुओं पर हुए हैं, मैं उनको भूल जाऊँ ? भूल जाऊँगा फिर उनकी पुनरावृत्ति कैसे की जा सकेगी ?’’
यह वार्तालाप नई दिल्ली में कर्जन रोड पर एक कोठी के ड्राइंग-रूम में, एक गद्देदार आराम-कुर्सी पर बैठ हुए अधेड़ आयु के पुरुष और उसके सामने खड़े हुए एक युवक में हो रहा था। युवक की आयु लगभग पच्चीस वर्ष की प्रतीत होती थी। युवक ने यह बात उस अधेड़ आयु के पुरुष के इस कथन के उत्तर में कही थी—
‘‘नरेन्द्र, देखो, तुम्हारी माता का देहान्त हो चुका है। तुम दो वर्ष के थे जब तुम्हारे पिता मारे गए थे। तब से तुम्हारी माता ने बहुत धैर्य और परिश्रम से तुम्हारा पालन-पोषण कर तुम्हें इतना बड़ा किया है। यह बीस-बाईस वर्ष की तपस्या किसलिए की गई थी ? इसलिए ही न कि तुम पढ़-लिखकर बड़े हो जाओ, विवाह करो और अपने पिता का वंश चलाओ। तुम्हारे लिए यही अवसर है कि तुम अपनी माँ की इच्छा पूर्ण कर उसकी पवित्र स्मृति को चिरस्थायी बनाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूढ़ी है। वह पढ़ी-लिखी है, सुन्दर है, सुशील है, सुघड़ है और अति मीठा बोलने वाली है। एक बार चलकर लड़की को देख लो। देखो, माँ के परिश्रम का स्वाभाविक फल यही है। वह बेचारी जीती होती तो बहू लाने की बात सुनकर कितना आनन्द का अनुभव करती।’’
युवक का कहना था कि, ‘‘चाचा जी, आप नहीं जानते कि माता जी ने मुझे पढ़ाया-लिखाया क्यों है। आप समझते हैं कि पिताजी का वंश को चलाना ही उनके इस प्रयास का ध्येय था। यह तो बहुत छोटी बात है। वे इस प्रकार के छोटे विचारों की स्त्री नहीं थीं। मैं आपको बताता हूँ। मैंने मैट्रिक पास करने के पाश्चात् एक बार उनसे कहा था, ‘‘माँ, तुम्हें मेरे लिए गरीबी सहन करनी पड़ रही है; यदि तुम कहो तो मैं कहीं नौकरी कर लूँ। अब कहीं-न-कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी।’
‘‘माता जी ने मेरी बात सुन, माथे पर त्योरी चढ़ाकर कहा था, ‘‘देखो, नरेन्द्र, तुम्हारे चाचा जो कुछ भेजते हैं उससे तो तुम्हारी फीस और किताबों का खर्च भी नहीं चलता। घर और शेष तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए मुझे कपड़े सीने का काम करना पड़ता है। तुम्हें अखाड़े में कसरत करके आने पर बादाम और दूध देने तथा तुम्हारे कपड़े और अन्य आवश्यक बातों के लिए मैं जो दिन-रात मेहनत कर रही हूँ वह क्या केवल तुम्हारे तीस रुपये मासिक का क्लर्क बनाने के लिए है ? तुम्हारे खाने, पहनने, पुस्तकों और स्कूल इत्यादि की फीस के लिए, रात-रात-भर बैठकर लोगों के कपड़े सी-सीकर, मैं अपनी आँखें इसलिए खराब नहीं कर रही कि तुम विदेशी सरकार की नौकरी करने के योग्य हो जाओ। देखो, बेटा, मैं तुम्हें सबल और योग्य इसलिए बना रही हूँ कि तुम अपने पिता और मेरे अपमान का बदला ले सको। मैं आज फिर तुम्हें उस अपमान की कहानी सुनाती हूँ।
‘सन् 1919, अप्रैल मास के दिन थे। महात्मा गांधी पंजाब आ रहे थे और पंजाब सरकार ने उन्हें आने से रोक दिया था। जब उन्होंने आने का हठ किया तो सरकार ने उन्हें बन्दी बना लिया। लोगों ने हड़ताल कर दी, जो कई दिन तक रही। उस समय तुम दो वर्ष के थे। तुम्हारे पिता हाल बाजार में बिसाती की दुकान करते थे। वे भी दुकान बन्द करके घर आ बैठे।
‘वैशाख की संक्रांति थी। उनके मन में आया कि ‘दरबार साहब’ में स्नान तथा दर्शन कर आवें। मैं भी साथ जाती, परन्तु तुम्हारी बहन, राधा, पेट में थी। अतएव मैं और तुम घर पर ही रहे और वे लोटा लेकर दरबार साहब चले गए। उनका विचार था कि अमृतसर के जल का लोटा भरकर मेरे और तुम्हारे लिए लावेंगे।
‘वे गए और फिर नहीं आए। सायंकाल तक मैं प्रतीक्षा करती रही। उनके न आने पर मैं बेचैन हो उठी। मुहल्ले में हल्ला मच गया कि जलियांवाला बाग में लोग जलसा कर रहे थे कि फौज ने गोली चलाकर सहस्रों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मेरा माथा ठनका। यद्यपि वे कभी ऐसे जलसे-जुलूसों में सम्मिलित नहीं होते थे, फिर भी मुझे विश्वास-सा होने लगा था कि वे वहीं पर मारे गए हैं। मैंने तुम्हें पड़ोसन के घर छोड़ा और जलियांवाला बाग को चल पड़ी। मुहल्ले के लोगों ने मना किया, पर मैं उतावली हो रही थी। वे कहते थे कि संध्या होने वाली है और ‘कर्फ्यू-आर्डर’ लगा हुआ है, किसी फौजी ने देख लिया तो वह गोली से मार डालेगा। मैं भगवान् के भरोसे पर थी। बाजार सुनसान पड़े थे। कोई पक्षी तक भी फड़क नहीं रहा था। मैं मकानों के साथ-साथ होती हुई चली गई। मेरे मन में अपने लिए भय नहीं था। मुझे विश्वास-सा हो रहा था कि तुम्हारे पिता जीवित नहीं हैं। जीवित होते तो अवश्य लौट आते। इस बात का निश्चय करना मेरे लिए नितान्त आवश्यक था। मैं चलती गई। तब तक प्रकाश पर्याप्त था, मैं वहाँ जा पहुँची।
‘जलियांवाले अहाते में जाने के दो मार्ग हैं। एक बड़ा फाटक-सा है, और दूसरे को तो केवल खिड़की ही कहना चाहिए। मैं फाटक के मार्ग से भीतर गई थी। सामने हाय-हाय मची हुई थी। हजारों लोगों के मुख से आर्त्तनाद निकल रहा था। कोई-कोई विरला उनमें खड़ा अपनी सम्बन्धियों को पहचान रहा था। ये अपने सम्बन्धियों को ढूँढ़ने वाले, कभी-कभी शवों को घसीटकर इधर-उधर करते थे। सूर्यास्त होने में कुछ मिनट ही रह गए थे और ढूँढ़ने वाले अनुभव कर रहे थे कि शीघ्र ही उनको लौट जाना है। सूर्यास्तके पश्चात् शव ले जाना तो एक तरफ रहा घर पहुँचना भी भय-रहित नहीं रह जावेगा।
‘मैं इस भयानक दृश्य को देख हतोत्साहित हो गई। मेरा दिल बैठने लगा और मैं अपनी टाँगों पर खड़ी न रह सकी। जहाँ मैं बैठी थी वहाँ समीप ही एक घायल पड़ा था। वह मुझे देखते ही पानी माँगने लगा। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी जाँघ में गोली लगी थी और वह हिल नही सकता था। वहाँ न लोटा था, न कुआँ। पानी लाती भी तो कहाँ से ? मेरे आँसू बहने लगे।
‘जिन ढूँढ़नेवालों को अपने आदमी मिल जाते थे वे उन्हें उठाकर चले जा रहे थे। उनमें से एक आदमी मुझे चुपचाप बैठे और रोते देख बोला, ‘माई, जल्दी चली जाओ। साढ़े सात बज रहे हैं। ‘कर्फ्यू आर्डर’ हो गया है’। इतना कहते-कहते वह रुक गया। वह खड़ा हो गया। शायद वह मेरी गर्भावस्था जान गया था और मन में कुछ सोचकर पूछने लगा, ‘‘तुम इसे कहाँ ले जाना चाहती हो ?’ उसने समीप पड़े घायल को मेरा सम्बन्धी समझ लिया था।
‘मैंने कहा, ‘इसे थोड़ा पानी पिला दो।’ मैं उसे होंठों पर जुबान फेरते देख तुम्हारे पिता के विषय में भूल गई थी। वह आदमी विचार में पड़ गया। बोला, ‘बहन, यहाँ पानी नहीं है। चलो, मैं इसे उठाकर ले चलता हूँ। आपको इसे कहाँ ले चलना है ?’
‘मुझे तुम्हारे पिता की याद आ गई। मैंने कहा, ‘‘इसे मैं नहीं जानती, मैं तो किसी और को ढूँढ़ने आयी थी।’
‘वह मिला ?’
‘नहीं, अभी नहीं। मुझ में यह सब ढूँढ़ने की हिम्मत नहीं रही।’
‘वह आपका क्या है ?’
‘मेरे पति हैं।’
‘उस भले पुरुष के मुख पर दया की झलक दिखाई दे रही थी। वह बोली, ‘चलो, उसे भी देख लो, बहन ! शायद उसे भी पानी की आवश्यकता हो।’
‘उसने मुझे आश्रय दे उठाया और हम ढूँढ़ने लगे। अहाते के एक ओर एक दीवार थी और सबसे अधिक लाशें उसी दीवार के समीप थी। एक स्थान पर लाशों का ढेर लगा था। मैं ढूँढ़ती हुई वहाँ पहुँची। उफ ! कितना भयंकर दृश्य। अब भी स्मरण आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक-एक शव को पकड़कर मुख देखती थी और पहचानती थी। जब निश्चय हो जाता था कि तुम्हारे पिता नहीं है, तो उन्हें घसीटकर एक तरफ कर देती थी और फिर दूसरों को देखती थी। सभी लोग इस प्रकार कर रहे थे। इस पर भी यह कार्य इतनी कठोरतापूर्ण था कि साधारण परिस्थिति में कोई अति कठोर-हृदय भी शायद वैसा ही कर सकता। मुझसे यह कुछ न हो सकता, यदि वह भला पुरुष मेरी सहायता न कर रहा होता। आखिर लाशों के एक ढेर के नीचे उनका शव निकला। उनके सिर में गोली लगी थी और खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए थे। उनका मुख पहचाना नहीं जाता था परन्तु कपड़ों से पहचान गई थी। उनको देख अपनी क्षीण सूत्रवत् आशा, कि शायद वे भी घायल पड़े हों, विलुप्त हुई जान में गश खाकर गिर पड़ी।
‘जब मुझे चेतना हुई तो वही भला आदमी मुख पर पान के छींटे लगा रहा था। अँधेरा पर्याप्त हो चुका था इसलिए पहले तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकी। इस समय उसके साथ एक आदमी था। वह हाथ में एक गगरा पानी लिये खड़ा था। जब पहचान गई तो मैंने पूछा, ‘उसे पानी पिलाया है, भैया ?’
‘बहिन जब तुम बेहोश हो गई थीं मैं पानी लेने चला गया था। मैंने विचार किया था कि तुम्हें सचेत करने के लिए भी तो पानी चाहिए। बाजार में कुआँ तो था पर गगरा नहीं था। एक मकान का दरवाजा खटखटाया और लोटा और गगरा माँगा। उस घर वालों ने एकदम इन्कार कर दिया। कई स्थानों पर यत्न करते-करते ये सज्जन मिले। घर पर ये अकेले थे। जब मैंने अपना आशय वर्णन किया, तो दाँतों को पीसते हुए गगरा और लोटा ले मेरे साथ चल पड़ा। इस सब प्रयत्न में एक घण्टा लग गया है, और इस बीच वह आदमी चल बसा है। अब उसकी सहायता नहीं कर सकते।’
‘मैं पगली-सी इन बातों को सुन रही थी। मुझे न तो अपनी जान का भय रह गया था और न ही उनके भय का अनुमान लगाने की मुझमें शक्ति रह गई थी। गगरा लिये हुए आदमी ने दूसरे घायलों को पानी पिलाना आरम्भ कर दिया। एक गगरे से वहाँ क्या हो सकता था। देखते-देखते पानी समाप्त हो गया। अब वह हमारे समीप आया और बोला, ‘माताजी, अब चलना चाहिए। आपको घर पहुँचा दूँ तो इनके लिए और जल का प्रबन्ध करूँ।’
‘मैंने अपनी गली का नाम बताया तो उन दोनों ने तुम्हारे पिता का शव कंधों पर उठा लिया और मुझे साथ ले घर पहुँचा गए। उस रात यद्यपि ‘कर्प्यू आर्डर’ लगा हुआ था, परन्तु तमाम अमृतसर में एक भी पुलिस तथा फौज का सिपाही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि ये लोग डर रहे थे कि उनके लिए शहर के भीतर आना मौत का आवाहन करना है। इस झूठे भय के कारण लोगों को रात के समय अपने घायल सम्बन्धी अथवा उनकी लाशें जलियांवाला बाग से ले जाने का अवसर मिल गया। प्रातःकाल तक कुछ लावारिस शवों के अतिरिक्त सहस्रों घायल तथा मृत वहाँ से ले जाए जा चुके थे।
‘दूसरे दिन केवल पाँच आदमियों की सहायता से तुम्हारे पिता का दाह संस्कार किया गया। श्मशान-भूमि तक जाने के लिए भी पाँच से अधिक लोगों का एकत्रित होना रोक दिया गया था।
‘जलियांवाला बाग में गोलियाँ चलाने वाला कर्नल डायर था। उस निर्दयी ने निहत्थे लोगों पर जो शान्तिपूर्वक जलसा कर रहे थे, तब तक गोलियां चलाई जब तक कि उसके सिपाहियों के कारतूस समाप्त नहीं हो गए।’
‘बात यहीं समाप्त नहीं हुई। हमारी गली के बाहर फौजियों का पहरा बैठ गया। वे आने-जाने वालों को पेट के बल रेंगने को बाध्य करते थे। हमारी गली वालों ने इस अपमान को न सह सकने के कारण घर से निकलना बन्द कर दिया। दुर्भाग्य से हमारे घर में रसद-पानी समाप्त हो गया। गली में प्रायः सब घरों का ऐसा ही हाल था। मैंने एक पड़ोसी से कुछ ला देने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। मैंने कहा, ‘‘नन्हा भूख से बिलख-बिलखकर रो रहा है।’ वह पड़ोसी चुप रहा उसके मुख पर विवशका की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। तुम्हें कुछ खाये चौबीस घंटे से ऊपर हो चुके थे। एक-दो बार तुम्हें पानी में चीनी घोलकर दिया। उससे तुम्हारी तृप्ति नहीं होती थी और फिर चीनी भी समाप्त हो गई थी। नगर में एक सप्ताह से ऊपर दूकानें बन्द रही थीं, और जब दूकानें खुलीं तो गली के बाहर यह आफत आ बैठी। परिणामस्वरूप उस गली में रहने वाले प्रायः सब फाके कर रहे थे। मैं माँगती भी तो किससे ? तब तुम बहुत रोने लगे तो मैंने इस अपमान को सहन करने की ठान ली। मेरे मन में पागलपन समा रहा था। मैं सोचती थी कि मैंने, तुमने और तुम्हारी बहन ने, जो अभी पेट में थी, उन लोगों का क्या बिगाड़ा है। वे मुझे रेंगेने के लिए क्यों कहेंगे ? मैंने कपड़े बदल लिये। सलवार, कुर्ता और दुपट्टा ओढ़ और हाथ में सामान के लिए चादर लेकर चल पड़ी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book